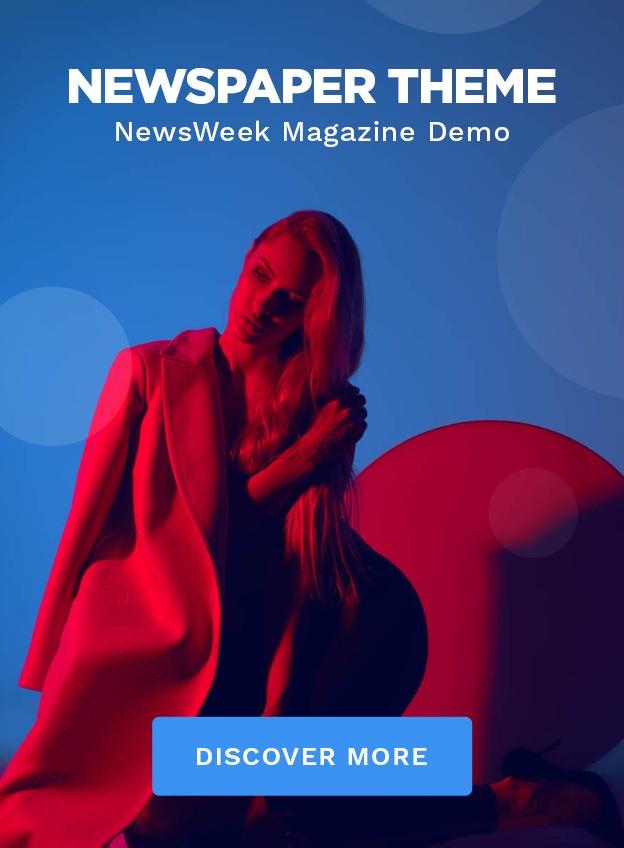इस वाक्यांश का इस्तेमाल अक्सर पड़ोसी देशों के बीच संबंधों की जटिलताओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, खासकर तब जब तनाव बढ़ जाता है। पड़ोसी जुड़वाँ बच्चों की तरह होते हैं, जो कुछ अपरिहार्य तत्वों को साझा करते हैं – प्राकृतिक आपदाएँ, बीमारियों का प्रसार, राजनीतिक अस्थिरता, सीमा पार तस्करी और अपराध जो आसानी से सीमाओं को पार कर जाते हैं। यहाँ तक कि अनजाने में हुई घटनाएँ, जैसे कि मछुआरे एक-दूसरे के क्षेत्रीय जल में चले जाना, ऐसे रिश्तों की पेचीदगियों को रेखांकित करती हैं।
इन मुद्दों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तंत्र कूटनीति है, जो संबंधित राजनयिकों द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से संचालित की जाती है। हालाँकि, जब सभी कूटनीतिक जुड़ाव विवादों को हल करने में विफल हो जाते हैं, तो सशस्त्र संघर्ष अक्सर अपरिहार्य हो जाता है। युद्ध के समय में भी, राजनयिक तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए पर्दे के पीछे अथक प्रयास करते हैं।
आम लोगों की नज़र में, एक सैनिक और एक राजनयिक के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट है: एक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा शांति का। जबकि विदेशी सैन्यकर्मी मेजबान देश में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ पैदा कर सकते हैं, राजनयिकों का आमतौर पर सद्भावना के दूत के रूप में स्वागत किया जाता है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना होता है। अपने कार्य को पूरा करने के बाद, राजनयिक अक्सर दोस्ती और सद्भावना की विरासत छोड़ जाते हैं – जब तक कि, निश्चित रूप से, उन्हें अवांछित व्यक्ति (पीएनजी) घोषित नहीं किया जाता है।
यूरोप और एशिया-प्रशांत के 12 देशों में लगभग 35 वर्षों तक राजनयिक के रूप में काम करने के बाद – जिनमें से सात राजदूत या उच्चायुक्त के रूप में थे, जिसमें तीन देशों में समवर्ती मान्यताएँ शामिल हैं – मैंने हमेशा अपने मुख्य मिशन को उन देशों के साथ बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के रूप में देखा।
मेरा दृष्टिकोण बांग्लादेश के हितों को स्वार्थी रूप से प्राथमिकता देना नहीं था, बल्कि मेजबान देश की आशाओं और आकांक्षाओं के लेंस के माध्यम से पारस्परिक लाभों की पहचान करना था। दृढ़ता के साथ, मैं दावा कर सकता हूँ कि मैं अपने दृष्टिकोण के माध्यम से अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रहा।
अपने पूरे करियर के दौरान और यहां तक कि सेवानिवृत्ति के बाद भी, मैंने कभी भी उन देशों के प्रति बुरी भावना नहीं रखी, जहां मैंने सेवा की। इसके बजाय, मैंने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से उनके सकारात्मक पहलुओं को उजागर करना जारी रखा है, जबकि स्थिर और संतुलित संबंधों की वकालत की है। मेरा मानना है कि मैंने अपने पीछे अधिकारियों और सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच सद्भावना का भंडार छोड़ा है।
एक राजनयिक को उनके गृह देश और मेजबान देश के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में अमेरिकी महावाणिज्यदूत आर्चर ब्लड, बांग्लादेश में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं।
अपनी सरकार की नीति को चुनौती देते हुए, उन्होंने लगातार वाशिंगटन से बंगाली स्वतंत्रता, लोकतंत्र और आजादी के लिए समर्थन करने का आग्रह किया। जबकि राष्ट्रपति निक्सन और विदेश मंत्री किसिंजर ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया, आर्चर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और अंततः अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
आज, जबकि निक्सन और किसिंजर को बांग्लादेश में उपहास के साथ देखा जाता है, आर्चर को अपार सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाता है।
वर्तमान की बात करें तो 5 अगस्त, 2024 को जब शेख हसीना अभूतपूर्व जन विद्रोह के चलते भारत भाग गईं, तब से भारत ने बांग्लादेश के प्रति अपना रुख अचानक “सबसे अच्छे दोस्त” से बदलकर “सबसे बुरे दुश्मन” कर लिया है।
यह कैसे और क्यों हुआ या दोषारोपण किए बिना, जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया है, वह है बांग्लादेश में कुछ पूर्व भारतीय उच्चायुक्तों का आचरण। तर्क की आवाज़ बनने के बजाय, कुछ लोगों ने भड़काऊ बयानबाजी का सहारा लिया है, जिससे पहले से ही अस्थिर स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ गई है।
उनकी टिप्पणियों को सुनकर, कोई भी सोच सकता है कि वे बांग्लादेश में तत्काल सैन्य हस्तक्षेप की वकालत कर रहे हैं। उनके झूठ, गलत सूचना और भ्रामक सूचना सनसनीखेज भारतीय मीडिया, मुख्यधारा और सामाजिक दोनों, के साथ प्रतिस्पर्धा करते दिखते हैं, क्योंकि वे खुद को हिंदुत्व के चैंपियन के रूप में पेश करते हैं।
इस तरह का व्यवहार अनुभवी राजनयिकों के लिए अनुचित है, जिन्हें बांग्लादेश में अपने नेटवर्क का उपयोग करके स्थिति को समझना चाहिए और अपनी सरकार को विवेकपूर्ण तरीके से काम करने की सलाह देनी चाहिए। दुर्भाग्य से, यह उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था।
हालांकि, सभी भारतीय राजनयिक ऐसे संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखते हैं।
भारत में उच्च नैतिक मानकों वाले प्रतिभाशाली राजनयिकों की भरमार है। ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे पुराने मित्र शिव शंकर मेनन हैं, जो भारत के पूर्व विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। 2013 में भारत की एक निजी यात्रा के दौरान, मैंने उनसे भारत की बांग्लादेश नीति के बारे में खुलकर बातचीत की थी।
मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी की कीमत पर भारत जिस एक-पक्षीय दृष्टिकोण को अपना रहा है, वह उल्टा पड़ेगा। उन्होंने मेरे आकलन से सहमति जताई और स्वीकार किया कि जब उन्होंने इस दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश की थी, तो एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति ने इस बदलाव का विरोध किया था। दुर्भाग्य से, भारत की नीति अपरिवर्तित रही, और इसके आक्रामक रुख ने बांग्लादेश के लिए मामले को और भी बदतर बना दिया, जो कि, ऐसा लगता है, भारत का असली इरादा था।
यह खेदजनक है कि, जबकि बांग्लादेश में भारत में प्रत्यक्ष अनुभव रखने वाले कई पूर्व राजनयिक हैं, उनमें से अधिकांश ने इस महत्वपूर्ण समय के दौरान चुप रहना चुना है। कुछ भारतीय राजनयिकों की प्रवृत्ति भी उतनी ही चिंताजनक है कि वे बांग्लादेश की हर कार्रवाई को भारत के लिए खतरे के रूप में देखते हैं – चाहे वह चीन से पनडुब्बी खरीदना हो या बुनियादी ढांचे के विकास पर सहयोग करना हो।
इस तरह के भ्रम ने न केवल भारत की छवि को उसके पड़ोस में धूमिल किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी उसकी प्रतिष्ठा को कम किया है। यह सही समय है कि भारत सरकार अपनी विदेश नीति, विशेष रूप से अपनी बहुप्रचारित “पड़ोसी पहले” नीति का पुनर्मूल्यांकन करे, जो एक तमाशा बन गई है।
जैसा कि बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार और सेना प्रमुख दोनों ने जोर दिया है, भारत और बांग्लादेश एक साझा भविष्य साझा करते हैं और आपसी प्रगति के लिए एक-दूसरे की जरूरत है। यह केवल संप्रभुता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में निहित आपसी समझ, सम्मान और सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
जिस प्रकार भारत के विदेश मंत्री अक्सर स्वायत्त विदेश नीति अपनाने के देश के अधिकार पर जोर देते हैं, उसी प्रकार बांग्लादेश को भी अपना रास्ता तय करने का संप्रभु अधिकार है।