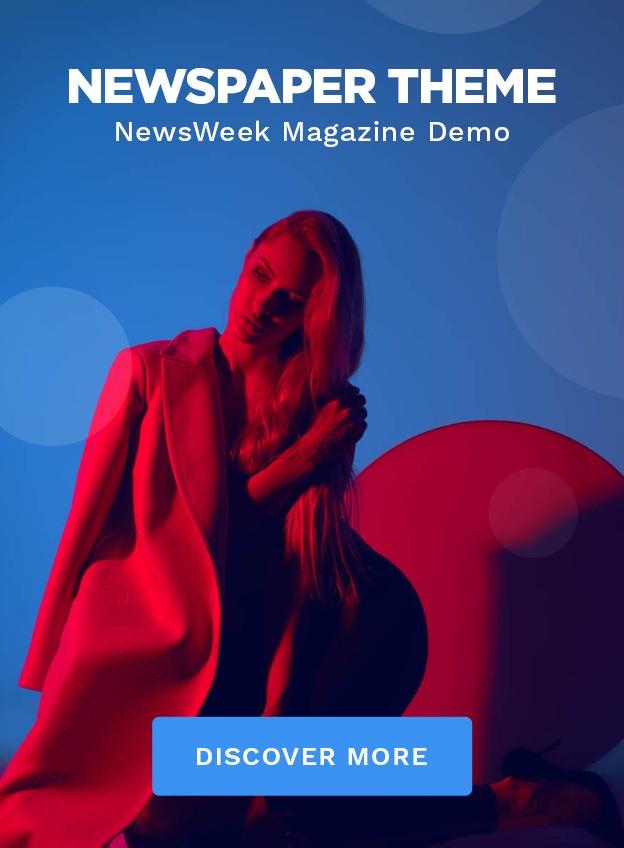दुनिया के शीर्ष 100 सबसे प्रदूषित शहर एशिया में हैं। नवंबर 2024 में नई दिल्ली समेत प्रमुख भारतीय शहरों और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में गंभीर वायु प्रदूषण बना रहा। स्थानीय निवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई और सर्दियों में धुंध की घटनाओं के परिणामस्वरूप स्कूलों और बाहरी निर्माण कार्यों को निलंबित कर दिया गया।
लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले और विकसित शहरों में वायु प्रदूषण कोई नई बात नहीं है। और प्रदूषित हवा के संपर्क में कहीं भी आ सकते हैं: चाहे कोई व्यक्ति कारखानों से भरे शहर से गुज़र रहा हो, भीड़-भाड़ वाले ट्रैफ़िक में फंसा हो या फिर किसी ग्रामीण इलाके में हो जहाँ गर्मी के लिए लकड़ी की आग पर निर्भर रहना पड़ता है।
हालांकि, दुनिया के सबसे बुरी तरह प्रभावित भागों में रहने वाले कई लोगों के लिए खराब गुणवत्ता वाली हवा से बचने के लिए सावधानी बरतना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है।
वायु प्रदूषण का कारण क्या है और यह धुंध कैसे बन जाता है?
स्मॉग “धुआं” और “कोहरा” का एक संयोजन है। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि यह गंदा, रासायनिक धुंध कैसे उत्पन्न होता है।
यह तब बनता है जब ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और अन्य जहरीले रसायन जैसे जमीनी स्तर के प्रदूषक सूर्य की रोशनी में कोहरे के साथ मिल जाते हैं।
धुँआ और वायु प्रदूषण खतरनाक क्यों हैं?
धुआँ और प्रदूषण खतरनाक हैं क्योंकि वे बहुत आसानी से साँस के ज़रिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
दहनशील प्रक्रियाएँ – चाहे औद्योगिक कारखाने में, आपकी कार के इंजन में या आपके घर की लकड़ी की भट्टी में – वातावरण में जहरीली गैसें छोड़ती हैं।
अक्सर धुएँ और गैस में सूक्ष्म कण होते हैं जो हमारे द्वारा जलाए जाने वाले पदार्थों के बीच जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप होते हैं।
कणिकाओं को आकार के अनुसार लेबल किया जाता है। उदाहरण के लिए:
2.5-10 माइक्रोमीटर आकार के कणों के लिए PM10
2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम आकार के कणों के लिए PM2.5
100 नैनोमीटर से कम आकार के अति सूक्ष्म कणों के लिए PM0.1
ये कण बहुत छोटे होते हैं। तुलना के लिए, एक मानव लाल रक्त कोशिका PM10 के आकार की सीमा में फिट हो सकती है क्योंकि वे लगभग 6-8 माइक्रोमीटर व्यास की होती हैं।
रोग पैदा करने वाले ई.कोली जैसे बैक्टीरिया लगभग 3 माइक्रोमीटर चौड़े होते हैं, इसलिए PM2.5 उससे भी छोटा होता है।
जहाँ तक अतिसूक्ष्म PM0.1 की बात है, ये कण इन्फ्लूएंजा और एचआईवी का कारण बनने वाले वायरस से भी छोटे होते हैं।
यह उनके सूक्ष्म आकार के कारण है कि इन रासायनिक कणों को साँस के साथ अंदर लेने से – जो जहरीली गैसों, भारी धातुओं और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं – रक्तप्रवाह में आसानी से अवशोषित हो सकते हैं, जहाँ वे दीर्घकालिक नुकसान पहुँचा सकते हैं।
स्वास्थ्य पर धुंध और वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं?
पार्टिकुलेट मैटर और प्रदूषक गैसों के साँस में जाने से लंबे समय से खराब स्वास्थ्य और कई तरह की बीमारियाँ और विकार जुड़े हुए हैं।
थोड़े समय के लिए प्रदूषण के संपर्क में आने से अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी समस्याएँ और संक्रमण जैसी गंभीर स्थितियाँ बढ़ सकती हैं और फेफड़ों की कार्यक्षमता ख़राब हो सकती है।
लंबे समय में, कैंसर, स्ट्रोक, हृदय और प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग जैसी पुरानी स्थितियाँ हो सकती हैं।
यह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति विशेष रूप से कमज़ोर होते हैं।
मई 2024 में, जर्मनी में कम उत्सर्जन वाले क्षेत्रों के एक अध्ययन में पाया गया कि जो बच्चे गर्भाधान से लेकर अपने पहले वर्ष तक स्वच्छ हवा के संपर्क में थे, उन्हें पाँच वर्ष की आयु से पहले दवा की ज़रूरत कम थी।
अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता हन्नाह क्लाउबर ने कहा, “इस शुरुआती जीवन अवधि में वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चों के बड़े होने पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं।”
पिछले अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जो बच्चे कम उम्र में प्रदूषण के संपर्क में आते हैं, वे स्कूल में कम प्रदर्शन करते हैं, कम टेस्ट स्कोर प्राप्त करते हैं और औसतन, वयस्क होने पर कम आय अर्जित करते हैं।
क्लाउबर ने डीडब्ल्यू को बताया, “हमने कई अध्ययनों में देखा है कि वायु प्रदूषकों का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है।” “मूल रूप से पार्टिकुलेट मैटर का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है, इसलिए पार्टिकुलेट मैटर में कोई भी वृद्धि प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ले जाती है।”
जबकि क्लाउबर का अध्ययन केवल जर्मनी पर केंद्रित था, क्लाउबर ने कहा कि उन्हें दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के परिणाम मिलने की उम्मीद है।
वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और क्यों?
वायु गुणवत्ता रेटिंग का उपयोग किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मानक की निगरानी के लिए किया जाता है।
इस तरह के रेटिंग पैमाने आमतौर पर राष्ट्रीय सरकारों द्वारा विकसित किए जाते हैं, इसलिए मानक देश-दर-देश अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन कई विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक सिफारिशों पर आधारित हैं।
कुछ देश और शहर अपनी गुणवत्ता रेटिंग को रंग-कोडित करते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और भारत में:
हरा रंग अच्छी गुणवत्ता वाली हवा के लिए है
पीला रंग मध्यम प्रदूषण के लिए है
नारंगी रंग खराब वायु गुणवत्ता के लिए है
लाल रंग बहुत खराब वायु गुणवत्ता के लिए है
धुंध से खुद को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ आप इससे बच नहीं सकते तो आप खुद को स्मॉग से प्रभावी रूप से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन नई दिल्ली और लाहौर जैसे कुछ उच्च प्रदूषण वाले शहरों में, अधिकारी बाहरी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसमें स्कूल बंद करना, कार और अन्य वाहन चलाने की सीमाएँ और बाहरी कामों को निलंबित करना शामिल है।
स्मॉग और उच्च वायु प्रदूषण वाले शहरों में निवासियों को जहाँ संभव हो फ़िल्टरेशन तंत्र का उपयोग करने और शारीरिक परिश्रम को कम करने की सलाह दी जा सकती है।
क्या स्कूल बंद करने से वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी?
नहीं, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रोफेसर राजीब दासगुप्ता के अनुसार ऐसा नहीं है। दासगुप्ता ने डीडब्ल्यू को बताया कि बाहरी गतिविधियों पर प्रतिबंध या स्कूल बंद करना केवल अस्थायी उपाय हैं। दासगुप्ता ने कहा, “यह ऐसी चीज है जिसे आप व्यक्तिगत या घरेलू स्तर के हस्तक्षेपों के माध्यम से नहीं संभाल सकते। यह ऐसी चीज है जिसके लिए राज्य की कार्रवाई और बहुत बड़ी बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई की आवश्यकता होती है।”
वायु प्रदूषण पर सख्त सीमाएँ लगाने के लिए दुनिया भर में कार्रवाई की जा रही है। यूरोपीय संघ ने जून 2024 में नए मानकों पर सहमति व्यक्त की और एशिया में वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास भी सबसे अधिक प्रभावित स्थानों जैसे कि बीजिंग, चीन में चल रहे हैं। बीजिंग के अधिकारियों ने 2013 में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को विद्युतीकृत करने की योजना पेश की। इससे धुंध और प्रदूषण में कुछ महत्वपूर्ण कमी देखी गई, लेकिन उनका स्तर अभी भी सरकारी और वैश्विक वायु गुणवत्ता सिफारिशों से ऊपर है। भारत ने भी नई स्वच्छ वायु नीतियाँ लागू की हैं, लेकिन दासगुप्ता ने प्रगति की कमी की आलोचना की: “ऐसा लगता है कि राज्य अपने कामों को एक साथ करने में सक्षम नहीं हैं, और यह पैसे की कमी के कारण नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति की कमी के कारण है।”